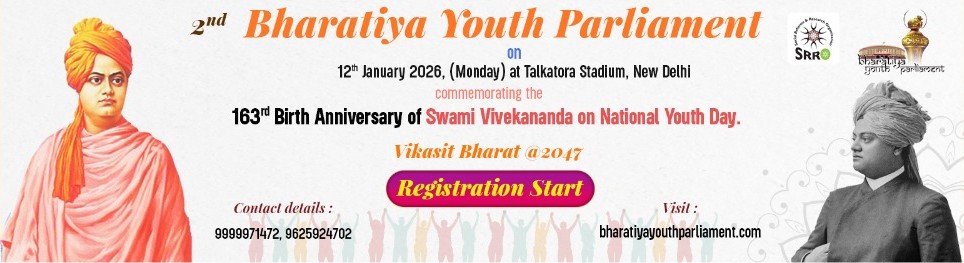प्रस्तावना
भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती ही समग्र विकास की बुनियाद है। जब गाँवों के लोग आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तभी भारत की प्रगति का सपना पूरा हो सकता है।
वर्ष 2005 में शुरू हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MGNREGA) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देना है — ताकि वह अपनी आजीविका सुरक्षित रख सकें।
हालाँकि, समय के साथ चुनौतियाँ बढ़ी हैं — मजदूरी की गिरावट, फंड की कमी, देनदारियाँ, योजनाओं की क्रियान्वयन गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, और बजट नियंत्रण।
2025-26 का बजट और हाल के फैसले यह संकेत देते हैं कि मनरेगा फंड में वृद्धि और संरचनात्मक सुधार किये जा रहे हैं।
इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि फंड वृद्धि की वजह क्या है, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक असर, चुनौतियाँ और सुझाव — और यह कैसे ग्रामीण रोजगार को नई गति दे सकती है।
मनरेगा फंड वृद्धि:
आंकड़े और बदलाव
बजट आवंटन और रिलीज़ की गई राशि
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा को कुल ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
जुलाई 2025 तक इस राशि में से लगभग ₹44,323 करोड़ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी कर दिए गए हैं।
यह राशि मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग की जा रही है।
मजदूरी दरों में वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2025-26 से मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ₹349 से बढ़ाकर ₹370 कर दी गई है।
विभिन्न राज्यों में यह वृद्धि 2.33% से लेकर 7.48% तक देखी गई है।
उदाहरण के लिए, हरियाणा में मजदूरी ₹400 तक पहुँच गई है।
खर्च पर नियंत्रण / कैप
यह पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा खर्च पर 60% की सीमा निर्धारित की है — यानी पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर) में कुल बजट का अधिकतम 60% ही खर्च हो सकता है।
लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पहले तीन महीनों (अप्रैल–जून) में ही 78% फंड खर्च हो गया, जो कि समस्या का संकेत है।
फंड वृद्धि का ग्रामीण रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव
फंड में कटौती के बजाय वृद्धि और मजदूरी दरों में सुधार से ग्रामीण रोजगार को कई तरह से नई गति मिल सकती है:
1. मांग में वृद्धि
जब मजदूरी दरें बढ़ती हैं, लोगों को काम करने का भूग बढ़ता है। गाँवों में अधिक लोग मनरेगा कार्यों की मांग करेंगे। इससे रिक्ति कम होगी और रोजगार स्तर बढ़ेगा।
2. खरीद शक्ति बढ़ेगी
जब मजदूरी बढ़ेगी, श्रमिकों के पास अधिक नकदी होगी। वे छोटे स्तर पर खर्च कर सकेंगे — खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि — जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग बढ़ेगी।
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण गतिविधियों में तेजी

मनरेगा के कार्य अक्सर बुनियादी बुनावट जैसे सड़क, जल संरक्षण, बाँध, नालियों, तालाब निर्माण व पुनरुद्धार आदि विषयों पर होते हैं। यदि फंड व मजदूरी बेहतर हों, तो इन कार्यों की गुणवत्ता और संख्या दोनों बढ़ सकती हैं।
4. स्थिर रोजगार का अवसर बढ़ना
जब गाँवों में काम उपलब्ध रहेगा, पलायन (माइग्रेशन) कम होगा। लोग अपने गाँवों में ही काम कर सकेंगे — इससे सामाजिक स्थिरता बढ़ेगी।
5. महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को लाभ
मनरेगा का उद्देश्य यह भी है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों आदि को रोज़गार मिले। बेहतर फंड व मजदूरी से उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की राह आसान होगी।
संभावित चुनौतियाँ और चिंताएँ
हर वृद्धि में जोखिम भी होते हैं — जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि नीति प्रभावी बनी रहे:
1. खर्च नियंत्रण से रोड़ा
कैप लगाने की व्यवस्था से, यदि फंड का उपयोग पहले ही खेल जाता है (जैसे पहली तीन महीनों में 78% खर्च) तो बाकी वर्ष में काम की कमी हो सकती है।
Kisan India
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय – वित्त मंत्रालय टकराव
जब राज्य स्तर पर काम का दबाव हो, लेकिन केंद्र से पैसे समय पर नहीं मिलें, तो कामों में रुकावट आ सकती है।
3. नियंत्रण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना
ज्यादा फंड और कामों की संख्या बढ़ने से भ्रष्टाचार, कार्य गुणवत्ता में गिरावट, भ्रष्ट निरीक्षण आदि की आशंका बढ़ जाती है।
4. नियमों में छेड़छाड़ के आरोप
कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मनरेगा नियमों में छेड़छाड़ कर रही है और 60% फंड को जल-संबंधी परियोजनाओं में इवेंटली खर्च कर रही है।
5. तकनीकी और संस्थागत समस्याएँ
जैसे जॉब कार्ड निष्क्रिय होना, डिजिटल ई-केवाईसी की बाधाएँ, मजदूरों का “मैं जिंदा हूँ” प्रमाण देना आदि। उदाहरणतः हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।
रणनीति और सुझाव — कैसे गति बनाए रखें
नीचे कुछ सुझाव दिए हैं जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि फंड वृद्धि न सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहे, बल्कि जमीन पर असर दिखाए:
1. गतिशील बजट रिलीज़
पूरी राशि को एक बार में ना जारी किया जाए, बल्कि मांग आधारित और समयानुसार रिलीज़ हो — ताकि खर्च नियंत्रित और संतुलित हो।
2. समय पर भुगतान और पारदर्शिता
मजदूरी का समय पर भुगतान हो, बिना देरी और बिचौलियों के। सोशल ऑडिट, फिट-ऑडिट, स्थानीय निगरानी समितियों को सशक्त किया जाए।
3. ग्राम स्तर पर योजना-निर्धारण को सशक्त करना
ग्राम सभा या ग्राम स्तर की समितियों को यह तय करने का अधिकार देना कि फंड कहां खर्च हो — ताकि स्थानीय प्राथमिकताएँ ही पहले उठें।
4. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
पंचायती राज, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम लेखा समितियाँ आदि को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे बेहतर प्रबंधन कर सकें।
5. तकनीकी संसाधन और निगरानी
GIS मैपिंग, मोबाइल-आधारित मॉनिटरिंग, ड्रोन से निरीक्षण आदि का उपयोग किया जाए।
6. क्रॉस-लिंकिंग योजनाएँ
मनरेगा को अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं (जल संरक्षण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सौर ऊर्जा) से जोड़ा जाए ताकि कामों में बेहतर समन्वय हो।
7. फंड अनुवर्ती (tracking) और रिपोर्टिंग
हर गाँव, ब्लॉक, जिला स्तर पर खर्च, प्रगति, असमाप्त कार्यों की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए।
निष्कर्ष
मनरेगा योजना, यदि सही रूप से लागू हो, अवसरों की सौगात है — यह न केवल ग्रामीण श्रमिकों को काम देती है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को भी मजबूत करती है। फंड वृद्धि, मजदूरी दरों की बढ़ोतरी और बेहतर प्रबंधन से यह संभव हो सकता है कि ग्रामीण रोजगार को वाकई नई गति मिले।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी, पारदर्शिता, स्थिर नीति, और निरंतर समीक्षा हो। यदि ये सब ठीक से हों, तो इस बदलाव की लहर पूरे भारत में ग्रामीण जीवन को बेहतर दिशा दे सकती है।


![]() KPR News Live
KPR News Live